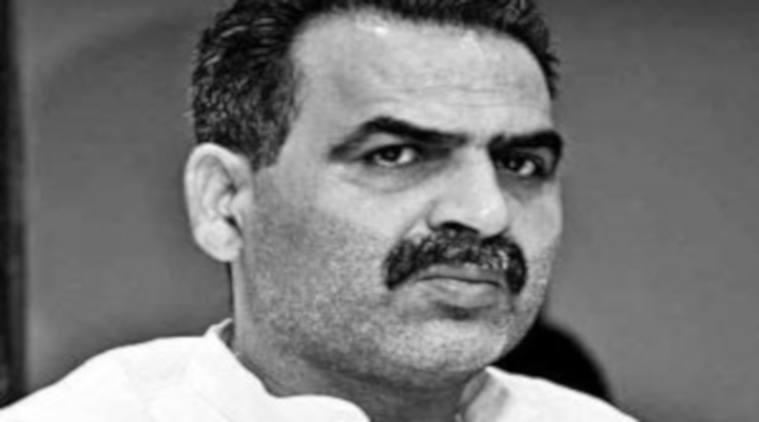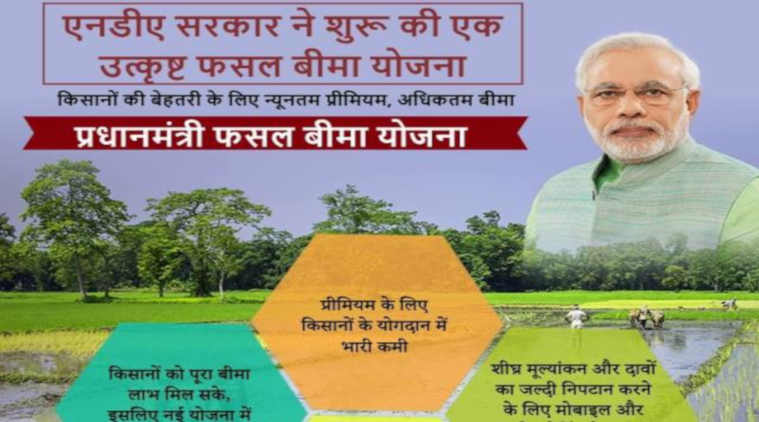Month: June 2016
सूखा – सच का या सोच का ?
आज सूखे की मार से दस राज्यों के 256 जिले और देश की एक तिहाई आबादी ग्रस्त है। कामधेनु की…
Tuesday, June 28, 2016मप्र: कर्ज तले दबे किसान ने एसिड पीकर दी जान
देश में कर्ज के बोझ तले किसानों की खुदकुशी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब मध्य के…
Tuesday, June 28, 2016टमाटर की महंगाई के बावजूद क्यों घाटे में रहा किसान?
टमाटर की कीमतों में आए उछाल ने देश की राजनीति को गरमा दिया। थोक मंडियों में आवक कम होने से…
Thursday, June 23, 2016वेटनरी कॉलेज खोलना होगा आसान, एक्ट में संशोधन की तैयारी
नई दिल्ली। देश में पशु चिकित्सकों कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार वेटनरी कॉलेज खोलने की राह आसान बनाने…
Tuesday, June 21, 2016शिमला: किसान नेताओं का अधिवेशन, छाया रहा किसान आय का मुद्दा
किसान एकता के बैनर तले शिमला में देश भर के किसान नेताओं का सम्मेलन चल रहा है। मौजूदा कृषि संकट…
Sunday, June 19, 2016कृषि मंत्रालय से बालियान की छुट्टी, अब 4 मंत्री करेंगे किसान कल्याण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को ताश के पत्तों की तरह फेट दिया है। 19 नए चेहरों को मंत्रिमंडल…
Sunday, June 19, 2016किसान ऋण मुक्ति: नितिन गडकरी ऐसे दूर करना चाहते हैं कृषि संकट
कृषि संकट और कर्ज के जंजाल से जूझ रहे किसानों को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कई…
Wednesday, June 15, 2016National Seminar on “Liberating the Farmers from Debt Trap”
According to 70th round of NSS data for the year 2012-13, majority of the farmers in India do not earn…
Tuesday, June 14, 2016कैसे उठाएंं प्रधानमंत्री बीमा योजना का फायदा? क्या हैं दिक्कतें?
करीब चार महीने पहले किसानों को प्रकृति की मार और अचानक होने वाले नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार…
Tuesday, June 14, 2016गेहूं पर आयात शुल्क वापस लेने की तैयारी, जानिए क्या होगाा असर?
केंद्र सरकार गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी के मद्देनजर आयात शुल्क वापस ले सकती है। फिलहाल गेहूं पर 25 फीसदी…
Saturday, June 11, 2016Top Videos

किसानों ने 27 राज्यों में निकाला ट्रैक्टर मार्च, अपनी लंबित माँगों के लिए ग़ुस्से में दिखे किसान

उत्तर प्रदेश के नोएडा के किसानों को शहरीकरण और विकास क्यों चुभ रहा है

Gig Economy के चंगुल में फंसे Gig Workers के हालात क्या बयां करते हैं?

Haryana में बाढ़ क्यों आयी? घग्गर नदी | मारकंडा नदी | टांगरी नदी