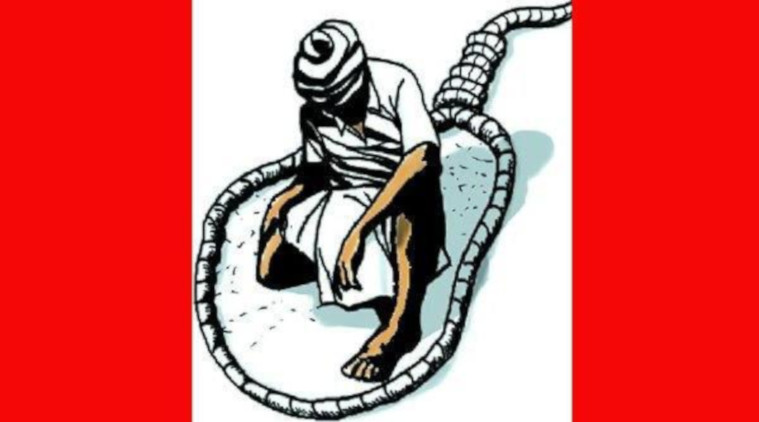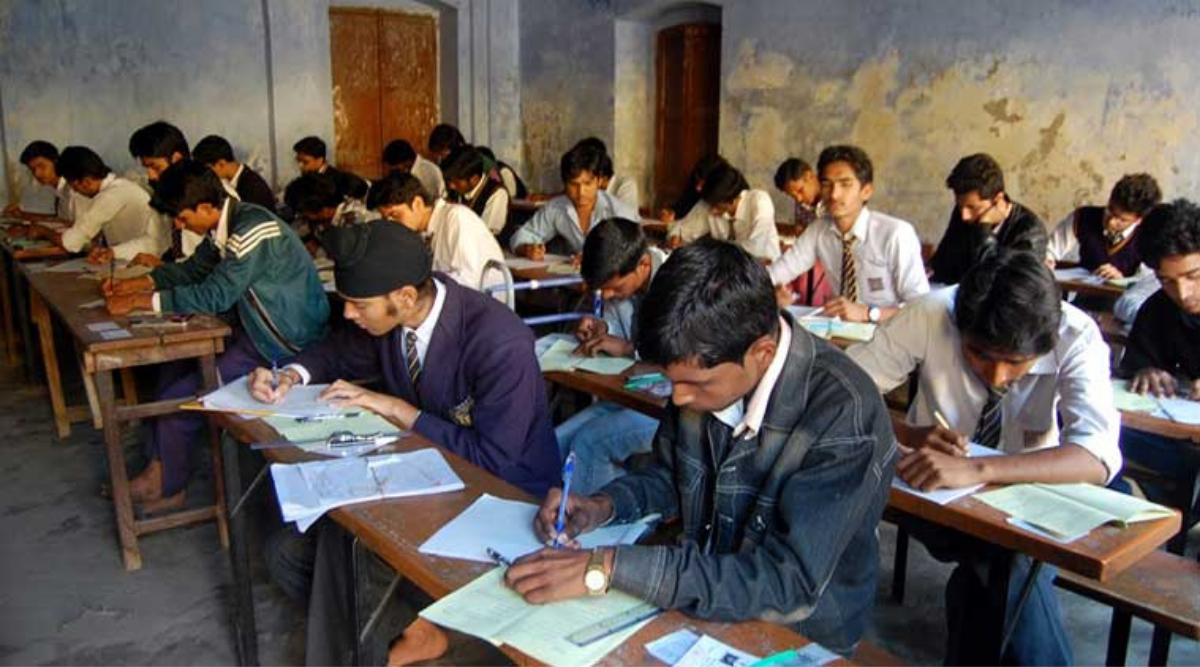Category: नवीनतम
पराली जलाने के आरोप में कैथल जिले के 14 किसान गिरफ्तार
हरियाणा के कैथल जिले में पिछले कुछ दिनों के भीतर अपने खेतों में पराली जलाने के आरोप में चौदह किसानों…
Monday, October 21, 2024पटियाला: मकान की छत गिरने से दो प्रवासी मजदूरों की मौत!
पटियाला में भारी बारिश के चलते एक मकान की छत गिरने से दो प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई.स्थानीय प्रशासन…
Wednesday, July 19, 2023उत्तर प्रदेश: बदायूं में अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर दो किसानों ने की आत्महत्या
न्याय की उम्मीद में यूपी के बदायूं जिले के दो किसानों की हिम्मत ने उस समय जवाब दे दिया जब…
Monday, June 26, 2023CMIE रिपोर्ट: बेरोजगारी में फिर पहले नंबर पर रहा हरियाणा, विपक्ष ने साधा निशाना!
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) की ओर से जारी बेरोजगारी दर के ताजा आंकड़ों में हरियाणा फिर से पहले…
Wednesday, January 4, 2023रिसर्च: सोशल मीडिया को लेकर युवाओं में बदलाव,फेसबुक जैसी एप्प पर घट रही सक्रियता!
प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा किए गए नए सर्वे में सामने आया है कि अमेरिका में अब युवा सोशल मीडिया से…
Saturday, September 10, 2022स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में खुलासा, खराब स्थिति में ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचा!
हाल ही में देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवीया ने ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ ढ़ांचे की स्थिति पर एक रिपोर्ट…
Wednesday, August 17, 2022आंधी-बारिश में यूपी के केला किसानों को भारी नुकसान, मुआवजा न मिलने से बढ़ी परेशानी!
पिछले 3 दिनों में मौसम के बदले मिजाज से उत्तर प्रदेश में गर्मी से झुलसते रोगों को राहत तो मिली,…
Monday, July 25, 2022पंजाब में Scholarship का भुगतान नहीं होने पर 2 लाख एससी छात्रों ने कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ी
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) ने बुधवार को कहा कि पंजाब सरकार द्वारा एक छात्रवृत्ति योजना (Scholarship Scheme) के तहत…
Thursday, July 21, 2022‘अग्निपथ’- योजना के विरोध में आन्दोलनकारी युवाओं ने हरियाणा को किया टोल मुफ्त, किसान संगठनों का भी मिला साथ
बीते कुछ दिन पहले केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद देश भर के युवाओं में योजना के…
Monday, June 20, 2022नागरिकों का सैन्यकरण या सेना का नागरिकीकरण?
तीन साल पहले (2019) लगभग इन्हीं दिनों, मीडिया के कुछ क्षेत्रों में सावधानीपूर्वक तैयार की गई एक महत्वपूर्ण खबर जारी…
Monday, June 20, 2022Top Videos

किसानों ने 27 राज्यों में निकाला ट्रैक्टर मार्च, अपनी लंबित माँगों के लिए ग़ुस्से में दिखे किसान

उत्तर प्रदेश के नोएडा के किसानों को शहरीकरण और विकास क्यों चुभ रहा है

Gig Economy के चंगुल में फंसे Gig Workers के हालात क्या बयां करते हैं?

Haryana में बाढ़ क्यों आयी? घग्गर नदी | मारकंडा नदी | टांगरी नदी