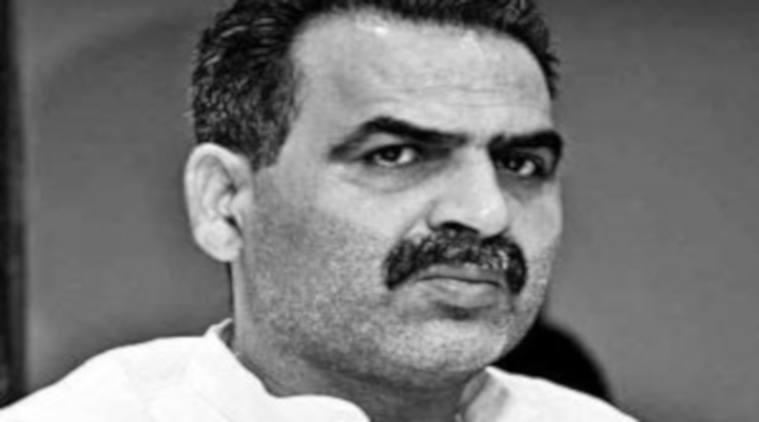Tag: किसान राजनीति
आंदोलनकारियों का चुनावी राजनीति में जाना: अन्ना आंदोलन से किसान आंदोलन तक के अनुभव
किसान आंदोलन स्थगित हो गया है लेकिन किसानों के कुछ संगठन और किसान नेताओं की तरफ से हरियाणा और पंजाब…
Wednesday, December 22, 2021राजनीतिक और आर्थिक परिदृष्य पर किसान लॉबी की वापसी
गुरू पर्व के मौके पर 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीन विवादास्पद कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा…
Thursday, November 25, 2021कृषि मंत्रालय से बालियान की छुट्टी, अब 4 मंत्री करेंगे किसान कल्याण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को ताश के पत्तों की तरह फेट दिया है। 19 नए चेहरों को मंत्रिमंडल…
Sunday, June 19, 2016Top Videos

किसानों ने 27 राज्यों में निकाला ट्रैक्टर मार्च, अपनी लंबित माँगों के लिए ग़ुस्से में दिखे किसान

उत्तर प्रदेश के नोएडा के किसानों को शहरीकरण और विकास क्यों चुभ रहा है

Gig Economy के चंगुल में फंसे Gig Workers के हालात क्या बयां करते हैं?

Haryana में बाढ़ क्यों आयी? घग्गर नदी | मारकंडा नदी | टांगरी नदी