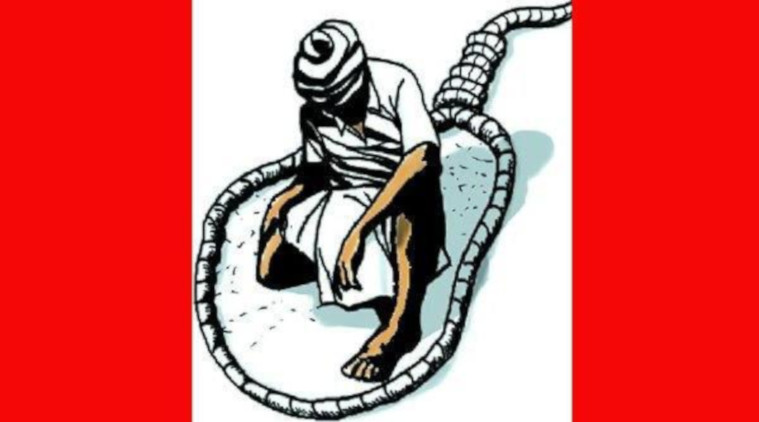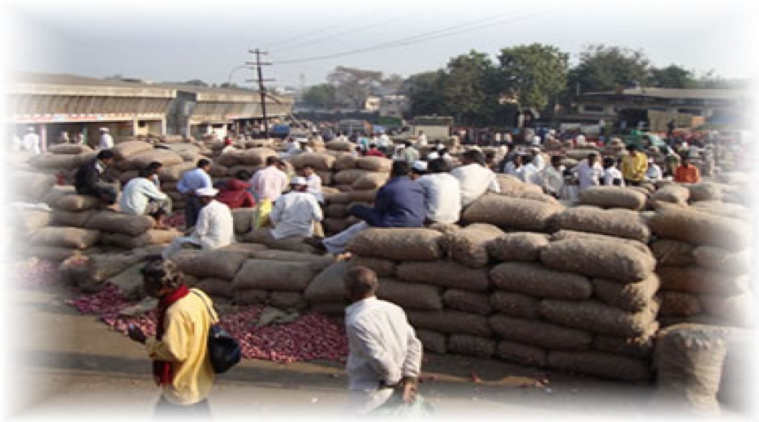Month: August 2016
सिंगुर फैसला: किसानों को बिना मुआवजा लौटाए वापस मिलेगी जमीन
किसान विरोधी भूमि-अधिग्रहण नीतियों को पश्चिम बंगाल में बड़ा झटका लगा है। टाटा मोटर्स के लिए सिंगुर में हुए भूमि…
Wednesday, August 31, 2016गुजरात: राजनीति और इंजीनियरिंग के लिहाज से क्यों खास है सौनी प्रोजेक्ट?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गुजरात के जामनगर पहुंचे और ‘सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण फॉर इरिगेशन’ (SAUNI) यानी सौनी प्रोजेक्ट के…
Wednesday, August 31, 2016यवतमाल: किसान बाप-बेटे ने एक ही पेड़ से लगाई फांसी
किसानों की आय दोगुनी करने के दावों और किसान कल्याण की तमाम योजनाओं के बावजूद देश में किसानों की खुदकुशी…
Thursday, August 25, 2016पासवान ने मिलों पर फिर बनाया चीनी कीमतें कम रखने का दबाव
गन्ना किसानों को उचित दाम और बकाया भुगतान दिलाने में नाकाम रहने वाली केंद्र सरकार चीनी मिलों पर लगातार कीमतेंं…
Saturday, August 13, 2016बैलगाड़ियों में लादकर किसानों ने राष्ट्रपति को पहुंचाईं अपनी समस्याएं
परेशानियों का बोझ हद से गुजरा तो पंजाब के किसानों ने अपनी बात राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तक पहुंचाने के लिए…
Thursday, August 11, 2016गांव की यादें और शहरों में अजनबी
समय आगे बढ़ता है और हम जैसे लोग अपने जीवन में हर वक्त इस विरोधाभास को सामने खड़ा पाते हैं।…
Wednesday, August 10, 2016दिखने लगा महाराष्ट्र के मंडी कानून में बदलाव का असर
टमाटर 30 रुपया किलो खीरा 15 रुपया किलो भिन्डी और करेला 40 रुपय किलो! सब्जियों के ये दाम मुंबई में…
Friday, August 5, 2016Top Videos

किसानों ने 27 राज्यों में निकाला ट्रैक्टर मार्च, अपनी लंबित माँगों के लिए ग़ुस्से में दिखे किसान

उत्तर प्रदेश के नोएडा के किसानों को शहरीकरण और विकास क्यों चुभ रहा है

Gig Economy के चंगुल में फंसे Gig Workers के हालात क्या बयां करते हैं?

Haryana में बाढ़ क्यों आयी? घग्गर नदी | मारकंडा नदी | टांगरी नदी